मीमांसा दर्शन में भावना एक पारिभाषिक शब्द है। भू धातु से प्रेरणा अर्थ में णिच् एवं ल्युट् प्रत्यय के संयोग से निष्पन्न भावना शब्द प्रेरणा अर्थ का बोधक है। मीमांसा दर्शन के अनुसार विधि का सम्बन्ध भावना से है। ‘भवितुर्भवनानुकूलो भावयितुर्व्यापारविशेषो भावना’ इस लक्षण वाक्य से भावना को परिभाषित किया गया है जिसका आशय है कि जो उत्पन्न होने वाला है उसकी उत्पत्ति के अनुकूल प्रयोजक का जो विशेष प्रकार का व्यापार है वही भावना है। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि चैत्र द्वारा देवदत्त को चावल बनाने के लिए प्रेरित किया जाना चैत्र का विशेष व्यापार है तथा चैत्र से प्रेरित होकर देवदत्त द्वारा चावल पकाने के प्रति किया गया अनुकूल विशेष व्यापार ही भावना है- ‘यथोत्पद्यमानस्यौदनस्योत्पत्त्यनुकूलो देवदत्तस्य व्यापारविशेषो भावनेत्यर्थः। यथा चोत्पद्यमानाया देवदत्तप्रवृत्तेरुत्पत्त्यनुकूलः प्रवर्तकः चैत्रस्याभिप्रायविशेषः’ इति। वैदिक उदाहरण में ‘यजेत स्वर्गकामः’ वाक्य से स्वर्ग की प्राप्ति करने हेतु याग में प्रवृत्ति अनिवार्य है। अतः यहाँ वैदिक वाक्य भावयिता है तथा जो स्वर्गप्राप्ति हेतु यागकर्म में प्रवृत्त होता है वह पुरुष भवितृ है। शास्त्रों में कहा भी है कि- ‘यथा वा ‘यजेत स्वर्गकामः’ इत्यत्रोत्पद्यमानस्य धात्वर्थस्य स्वर्गस्य वोत्पत्त्यनुकूलः स्वर्गकामस्य व्यापार उत्पद्यमानायाश्च स्वर्गकामप्रवृत्तेरुत्पत्त्यनुकूलो लिङो व्यापारविशेषः। तथा चान्योत्पादनानुकूलो भावुकस्य व्यापारविशेषो धात्वर्थादन्यः सर्वधात्वर्थसम्बद्धाकारेण भासमानो भावनासामान्यमिति सिद्धम्’।
‘यजेत स्वर्गकामः’ इस प्रवृत्त्यर्थक वाक्य में ‘यजेत’ पद विशेष वर्णनीय है, यजेत पद में मुख्यतः दो अंश हैं- यजि धातु एवं त प्रत्यय। त प्रत्यय में भी दो अंश हैं- आख्यातत्व एवं लिङ्त्व। आख्यातत्व दशों लकारों में विद्यमान होता है किन्तु लिङ्त्व केवल लिङ्लकार में ही होता है। शास्त्रों में आख्यातत्व एवं लिङ्त्व के सम्मिलित रूप को ही भावना कहा गया है- ‘उभाभ्यामप्यंशाभ्यां भावनैवोच्यते’।
भावना मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है- शाब्दी भावना एवं आर्थीभावना। शाब्दीभावना को ‘पुरुषप्रवृत्त्यनुकूलो भावयितुर्व्यापारविशेषो शाब्दीभावना’ अर्थात् किसी पुरुष की प्रवृत्ति के अनुकूल प्रयोजक (उपदेशक) द्वारा किया गया विशेष प्रकार का व्यापार ही शाब्दीभावना है। जैसे कि एक वृद्ध द्वारा किसी पुरुष से ‘गामानाय’ इस प्रकार से कहा जाता है उस वृद्ध की बात सुनकर पुरुष के मन में विचार आता है कि इस वृद्ध द्वारा मुझे गौ लाने रूपी कार्य में प्रवृत्त किया जा रहा है तथा वह पुरुष तद्वत कार्य करता है। वृद्ध के ‘गामानय’ वाक्य से पुरुष द्वारा गौ लाने की क्रिया तक का व्यापार शाब्दीभावना कहलाता है। यह शाब्दीभावना प्रत्यय के लिङ्त्व अंश से द्योतित होती है। शाब्दीभावना में होने वाला व्यापार पुरुषनिष्ठ एवं शब्दनिष्ठ हो सकता है लौकिक वाक्यों में पुरुषनिष्ठ तथा वैदिकवाक्यों में शब्दनिष्ठ होता है- ‘स च व्यापारविशेषो लौकिकवाक्ये पुरुषनिष्ठोऽभिप्रायविशेषः। वैदिकवाक्ये तु पुरुषाभावाल्लिङ्गादिशब्दनिष्ठ एव’। शाब्दीभावना में तीन अंशों की आकाङ्क्षा होती है- साध्य, साधन एवं इतिकर्त्तव्यता। साध्य की आकांक्षा होने पर आर्थीभावना के तीनों अंशों का अन्वय होता है- ‘तत्र साध्याकाङ्क्षायां वक्ष्यमाणांशत्रयोपेता आर्थीभावना साध्यत्वेनान्वेति’। साधन अंश की आकांक्षा होने पर लिङादिज्ञान का अन्वय होता है- ‘साधनाकाङ्क्षायां लिङादिज्ञानं करणत्वेनान्वेति’। तथा इतिकर्त्तव्यता की आकांक्षा होने पर अर्थवाद का अन्वय हो जाता है- ‘इतिकर्त्तव्यताकाङ्क्षायामर्थवादज्ञाप्यप्राशस्त्यमितिकर्त्तव्यतात्वेनान्वेति’।
आर्थीभावना का ‘प्रयोजनेच्छाजनितक्रियाविषयव्यापार
आर्थीभावना’ लक्षण है। जिसका आशय है कि स्वर्गादि प्रयोजन की प्राप्ति के
अनुकूल यागादि कर्म प्रकारक विशेष मानसिक व्यापार ही आर्थीभावना कहलाता है। यह
आर्थीभावना प्रत्यय के आख्यातत्व अंश से व्यक्त होती है। आर्थीभावना में भी साध्य,
साधन एवं इतिकर्त्तव्यता ये तीन आकाङ्क्षायें होती हैं जहाँ स्वर्गादि फल ही साध्य
के रूप में अन्वित होता है- ‘साध्याकाङ्क्षायां स्वर्गादिफलं
साध्यत्वेनान्वेति’। साधन की आकाङ्क्षा होने पर यागादि कर्म का अन्वय होता है-
‘साधनाकाङ्क्षायां यागादिः करणत्वेनान्वेति’। तथा प्रयाजादि अङ्ग ही
इतिकर्त्तव्यता के रूप में अन्वित होते हैं- ‘इतिकर्त्तव्यताकाङ्क्षायां
प्रयाजाद्यङ्गजातमितिकर्त्तव्यतान्वेति’।
निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भावना मीमांसा दर्शन का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रतिपाद्य विषय है। किसी भी कर्म के सम्पादन में पुरुष की प्रवृत्ति अत्यन्त आवश्यक है। भावना के दो भेद शाब्दीभावना एवं आर्थीभावना पुरुष की प्रवृत्ति में अत्यन्त उपादेय हैं। पुरुषनिष्ठ एवं शब्दनिष्ठ के भेद से लौकिक वाक्य एवं अलौकिक वाक्य के द्वारा पुरुष की प्रवृत्ति द्रष्टव्य है। अतः कर्म मीमांसा नाम से प्रसिद्ध मीमांसा दर्शन में प्रयोजन की सिद्धि के लिए कर्म में प्रवृत्त करने वाला भावना सिद्धान्त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।
कृपया कमेण्ट, शेयर एवं फॉलो जरूर करें...
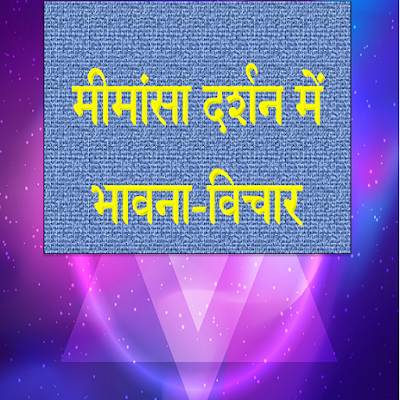
एक टिप्पणी भेजें